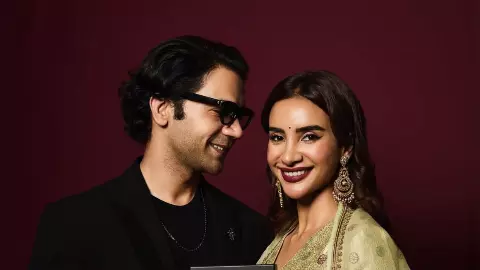Passive Euthanasia: क्या है पैसिव यूथेनेशिया? एक बार फिर क्यों चर्चा में, भारत में मर्सी किलिंग पर क्या है कानून
सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शानबाग को 2011 में इच्छा मृत्यु की इजाजत नहीं दी थी. हरीश ने भी अपने पिता के जरिए शीर्ष अदालत से निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी थी. अदालत ने इस पर विचार करने के लिए हॉस्पिटल से मेडिकल बोर्ड गठित करने और कम से कम समय में सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट देने को कहा है. उसके बाद से भारत में पैसिव यूथेनेशिया फिर चर्चा में है. जानें क्या होती है मर्सी किलिंग, किन हालात में दी जाती है अनुमति और भारत में सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए क्या नियम तय किए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु के एक मामले में 26 नवंबर को सुनवाई की. जस्टिस जेबी परदीवाला की अगुवाई वाली बेंच ने नोएडा के सेक्टर 39 के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को दो हफ्ते के अंदर एक सीलबंद लिफाफे में मेडिकल असेसमेंट जमा करने का निर्देश दिया. शीर्ष अदालत ने नोएडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से एक पिता की अर्जी की जांच करने के लिए 'डॉक्टरों का एक प्राइमरी बोर्ड' बनाने को कहा, जिसमें उसने अपने 31 साल के बेटे के लिए पैसिव यूथेनेशिया की मांग की है. बेटा 100% दिव्यांग है और पिछले 12 सालों से हमेशा के लिए वेजिटेटिव स्टेट में है.
कोर्ट ने लाइफ-सपोर्ट हटाने के बारे में जांच को बताते हुए कहा, "हम प्राइमरी बोर्ड को, जिसे (हॉस्पिटल द्वारा) बनाया जा सकता है, हमें एक रिपोर्ट देने का निर्देश देते हैं कि क्या लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट रोका जा सकता है या दूसरे शब्दों में वापस लिया जा सकता है." मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी. उसके बाद से निष्क्रिय इच्छामृत्यु का मसला एक बार फिर चर्चा में हैं.
अर्जी हरीश के पिता अशोक राणा ने दी थी. हरीश अगस्त 2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी में B Tech करते समय अपने PG अकोमोडेशन की चौथी मंजिल से गिरने के बाद क्वाड्रीप्लेजिक हो गया था. तब से उसे कई हॉस्पिटल ले जाया गया और अब उसे सांस लेने और न्यूट्रिशन के लिए ट्यूब का सहारा दिया जाता है. इससे पहले भी ऐसा ही एक मसला अरुणा शानबाग का अदालत के सामने 2011 में भी आया था.
कौन थीं अरुणा शानबाग, जिसकी याचिका अदालत ने ठुकरा दी?
मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल (केईएम) हॉस्पिटल में दवाई का कुत्तों पर एक्सपेरिमेंट करने का डिपार्टमेंट था. इसमें नर्स कुत्तों को दवाई देती थीं. उन्हीं में एक थीं अरुणा शानबाग. 27 नवंबर 1973 को अरुणा ने ड्यूटी पूरी की और घर जाने से पहले कपड़े बदलने के लिए बेसमेंट में गईं. वार्ड ब्वॉय सोहनलाल पहले से वहां छिपा बैठा था. उसने अरुणा के गले में कुत्ते बांधने वाली चेन लपेटकर दबाने लगा. छूटने के लिए अरुणा ने खूब ताकत लगाई. पर गले की नसें दबने से बेहोश हो गईं. अरुणा कोमा में चली गईं और कभी ठीक नहीं हो सकीं.
कोर्ट ने क्यों ठुकरा दी पिटीशन?
8 मार्च 2011 को अरुणा को दया मृत्यु देने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी. वह पूरी तरह कोमा में न होते हुए दवाई, भोजन ले रही थी. डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर अरुणा को इच्छा मृत्यु देने की इजाजत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पिटीशनर पिंकी वीरानी का इस मामले से कुछ लेना-देना नहीं है, क्योंकि अरुणा की देखरेख केईएम हॉस्पिटल कर रहा है.
अरुणा शानबाग के माता-पिता नहीं हैं. उनके रिश्तेदारों को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रही. केईएम हॉस्पिटल ने कई सालों तक दिन-रात अरुणा की बेहतरीन सेवा की है. लिहाजा, अरुणा के बारे में फैसले करने का हक केईएम हॉस्पिटल को ही है.
42 साल तक रही कोमा में
अरुणा शानबाग 42 साल तक कोमा में रहने के बाद 18 मई 2015 को मौत हो गई. अरुणा 1973 में मुंबई के केईएम हॉस्पिटल में रेप की शिकार हुई थीं.
यूथेनेशिया का इतिहास
इच्छामृत्यु, रोगी की पीड़ा को सीमित करने के लिये उसके जीवन को समाप्त करने की व्यवस्था है. भारत में कानूनी रूप से इसकी इजाजत किसी को नहीं है.
इच्छामृत्यु के प्रकार
सक्रिय इच्छामृत्यु (Active Euthanasia):
सक्रिय इच्छामृत्यु तब होती है जब चिकित्सा पेशेवर या कोई अन्य व्यक्ति जानबूझकर ऐसा कुछ करता है जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है, जैसे घातक इंजेक्शन देना.
निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia):
निष्क्रिय इच्छामृत्यु चिकित्सा उपचार को रोकने या वापस लेने का कार्य है, जैसे कि किसी व्यक्ति को मरने की अनुमति देने के उद्देश्य से जीवन समर्थक उपकरणों को बंद कर देना या वापस लेना है.
भारत में इच्छामृत्यु
भारत में सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2018 केस में एक ऐतिहासिक निर्णय में एक व्यक्ति के सम्मान के साथ मरने के अधिकार को मान्यता देते हुए कहा कि एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति निष्क्रिय इच्छामृत्यु का विकल्प चुन सकता है. इसके साथ ही असाध्य रूप से बीमार रोगियों द्वारा बनाई गई ‘लिविंग विल’ के लिए गाइडलाइन भी तय किए. इससे पहले वर्ष 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने अरुणा शानबाग मामले में पहली बार निष्क्रिय इच्छामृत्यु को मान्यता दी थी, लेकिन इसकी शर्तों के अनुरूप अभी तक किसी को इच्छा मृत्यु का लाभ नहीं मिला है.
शीर्ष अदालत ने कहा था कि "मृत्यु की प्रक्रिया में गरिमा, अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है. किसी व्यक्ति को जीवन के अंत में गरिमा से वंचित करना व्यक्ति को एक सार्थक अस्तित्व से वंचित करना है."
SC की संशोधित गाइडलाइन 2023
2023 में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय की थी, जिसमें अस्पतालों को परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में मरीजों की जांच के लिए डॉक्टरों का एक प्राइमरी बोर्ड बनाने का निर्देश दिया गया था. अगर प्राइमरी बोर्ड मेडिकल इलाज रोकने या वापस लेने को सर्टिफाइड करना है, तो एक सेकेंडरी बोर्ड को मामले की फिर से जांच करनी होगी। सिर्फ अगर सेकेंडरी बोर्ड पहले की राय को मान लेता है, तो अस्पताल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट और मरीज के परिजनों को बताने के बाद इलाज रोकने या वापस लेने की कार्रवाई कर सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने साल 2023 में 2018 के इच्छामृत्यु दिशानिर्देशों को संशोधित कर दिया. ताकि गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु प्रदान करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके. वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने सम्मान के साथ मृत्यु के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी. इस अधिकार को लागू करने के लिए असाध्य रूप से बीमार रोगियों के लिए दिशा निर्देश तय किए.
लिविंग विल का सत्यापन
एक दस्तावेज जिसमें कोई व्यक्ति यह बताता है कि वह भविष्य में गंभीर बीमारी की हालत में किस तरह का इलाज कराना चाहता है. इसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट के सत्यापन की आवश्यकता को हटा दिया गया है. अब, नोटरी या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापन ही पर्याप्त है, जिससे व्यक्तियों के लिए अपने जीवन को समाप्त करने के विकल्प को व्यक्त करने की प्रक्रिया सरल हो गई.
नेशनल हेल्थ डिजिटल रिकॉर्ड के साथ एकीकरण
पहले, लिविंग विल को जिला न्यायालय द्वारा संरक्षित रखा जाता था. संशोधित दिशा-निर्देशों में यह अनिवार्य किया गया है कि यह दस्तावेज राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड का हिस्सा हों. इससे देश भर के अस्पतालों और डॉक्टरों के लिए सरल पहुंच सुनिश्चित होती है, जिससे समय पर निर्णय लेने में सुविधा होती है.
इच्छामृत्यु से इनकार के लिए अपील प्रक्रिया
यदि किसी अस्पताल का मेडिकल बोर्ड जीवन रक्षक प्रणाली हटाने की अनुमति देने से इनकार करता है, तो रोगी/मरी का परिवार संबंधित उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है. इसके बाद न्यायालय मामले का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए नया मेडिकल बोर्ड गठित करेगा. ताकि मामले की गहन और न्यायपूर्ण समीक्षा सुनिश्चित की जा सके.
इच्छामृत्यु से जुड़े नैतिक पहलू
इच्छामृत्यु में व्यक्तिगत स्वायत्तता का सम्मान करना शामिल है, जिसका अर्थ है कि लोगों को अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए. विशेष रूप से यदि वे मानसिक रूप से सक्षम हैं तो पीड़ा को समाप्त करने का अधिकार होना चाहिए.
इसके लिए सहमति की भी आवश्यकता होती है, जिसमें व्यक्ति को अपनी स्थिति, इच्छामृत्यु की प्रक्रिया और इसके परिणामों को पूरी तरह से समझना चाहिए. ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उस पर दबाव नहीं डाला जा रहा है या उसके साथ किसी भी प्रकार का छल-कपट नहीं किया जा रहा है.
इच्छामृत्यु पर बहस जीवन की गुणवत्ता बनाम जीवन की शुचिता पर केंद्रित होता है. जीवन की गुणवत्ता में यह तर्क दिया जाता है कि कि पीड़ा को समाप्त करना और गंभीर बीमारी के दौरान अपनी गरिमा को संरक्षित करना नैतिक हो सकता है. जबकि जीवन की शुचिता या पवित्रता अक्सर धार्मिक या दार्शनिक मान्यताओं को दर्शाती है जिसके तहत यह माना जाता है कि जीवन आंतरिक रूप से मूल्यवान है और इसे समय से पहले समाप्त नहीं किया जाना चाहिए.
किन-किन देशों में इच्छामृत्यु की इजाजत
- नीदरलैंड, लक्जमबर्ग, बेल्जियम किसी भी ऐसे व्यक्ति, जो "असहनीय पीड़ा" का सामना करता है और उसके स्वास्थ्य में सुधार की कोई संभावना नहीं है, को इच्छा मृत्यु एवं सहायता प्राप्त आत्महत्या दोनों की अनुमति है.
- स्विट्जरलैंड में इच्छामृत्यु प्रतिबंधित है लेकिन किसी डॉक्टर या चिकित्सीय पेशेवर की उपस्थिति तथा सहायता से मृत्यु प्राप्त करने की अनुमति है.
- वर्ष 1942 से स्विट्जरलैंड ने सहायता प्राप्त आत्महत्या की अनुमति दी है, जिसमें व्यक्तिगत पसंद और मरने की प्रक्रिया पर नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया गया है. कानून के अनुसार व्यक्तियों का मस्तिष्क स्वस्थ होना चाहिए और निर्णय स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों से प्रेरित नहीं होना चाहिए.
- ऑस्ट्रेलिया ने भी दोनों प्रकार की इच्छा मृत्यु को वैध कर रखा है. यह उन वयस्कों पर लागू होता है जिनमें पूर्ण निर्णय लेने की क्षमता है तथा वे ऐसी लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हैं जिनकी छह या बारह महीनों के भीतर मृत्यु होने की संभावना है.
- नीदरलैंड में इच्छामृत्यु के लिए एक सुस्थापित विधिक ढांचा है, जिसे वर्ष 2001 के अनुरोध पर जीवन की समाप्ति और सहायता प्राप्त आत्महत्या अधिनियम द्वारा विनियमित किया जाता है.