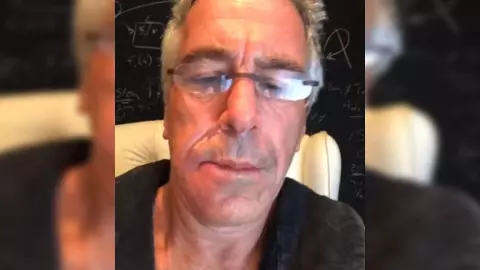अब जरूरत नहीं मां के कोख की! जापान ने बनाया दुनिया का पहला कृत्रिम गर्भ, लैब में शुरू हुआ इंसानी जीवन का सफर
जापान ने दुनिया को हैरान कर देने वाली तकनीक पेश की है. एक ऐसा कृत्रिम गर्भ जिसमें शरीर के बाहर भ्रूण विकसित हुआ. अब बच्चे पैदा करने के लिए मां की कोख जरूरी नहीं. ये खोज सिर्फ विज्ञान की नहीं, समाज, नैतिकता और इंसानी रिश्तों की परिभाषा भी बदलने वाली है. क्या यह भविष्य का जनमंत्र है या एक नई बहस की शुरुआत?

सोचिए, बिना किसी महिला के गर्भ के किसी इंसानी भ्रूण का जन्म और विकास हो सके, वो भी पूरी तरह मशीनों की देखरेख में. सुनने में भले ही यह एक फिल्मी कल्पना लगे, लेकिन जापान के वैज्ञानिकों ने इसे हकीकत बना दिया है. जुंटेन्डो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा कृत्रिम गर्भाशय विकसित किया है, जिसमें स्तनधारी भ्रूण को शरीर के बाहर पालना संभव हो गया है. यह पहली बार है जब जीवन की शुरुआत को पूरी तरह शरीर के बाहर, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में संचालित किया गया है. इस तकनीक को वैज्ञानिक भाषा में “एक्टोजेनेसिस” कहा जाता है. यह प्रयोग अभी तक बकरियों के भ्रूणों पर सफल रहा है, लेकिन इंसानी उपयोग की दिशा में पहला बड़ा कदम बन चुका है.
ये तकनीक जितनी अद्भुत है, उतनी ही सवालों से भरी भी है. अगर इंसानी शरीर की जगह मशीन मां बन सकती है, तो फिर माता-पिता बनने की परिभाषा भी बदल जाएगी. अब वो समय दूर नहीं जब कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष, या कोई कपल जो शारीरिक रूप से बच्चा नहीं कर सकता. वे भी संतान पा सकेंगे. लेकिन क्या हम इसके लिए मानसिक, सामाजिक और कानूनी तौर पर तैयार हैं?
कैसे काम करता है यह ‘लैब गर्भ’?
यह कृत्रिम गर्भ कोई साधारण डब्बा नहीं है. यह एक पारदर्शी जैविक थैली (बायोबैग) है जिसमें ऑक्सीजन और पोषक तत्त्वों से भरा विशेष एमनियोटिक तरल होता है. इसमें एक कृत्रिम गर्भनाल जोड़ा गया है जो भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन देता है. ठीक उसी तरह जैसे असली गर्भ में प्लेसेंटा करता है. इस सिस्टम में सेंसर लगे होते हैं जो भ्रूण की हर हलचल, दिल की धड़कन और उसके विकास पर नजर रखते हैं. इन सेंसरों को कंट्रोल करता है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम, जो भ्रूण की ज़रूरत के अनुसार तुरंत प्रतिक्रिया देता है. इसे देखकर लगता है मानो मेडिकल साइंस और रोबोटिक्स मिलकर मां बनने की जिम्मेदारी उठा रहे हों.
पहले भी हुए थे प्रयोग, लेकिन यह कदम सबसे आगे
2017 में अमेरिका के चिल्ड्रेन हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया ने भी एक प्रयोग किया था, जिसमें समय से पहले जन्मे मेमनों को एक कृत्रिम गर्भ में कुछ समय तक जिंदा रखा गया था. लेकिन वहां भ्रूण पहले से विकसित हो चुका था. जापान की नई सफलता में भ्रूण की शुरुआत और उसका शुरुआती विकास पूरी तरह लैब में हुआ है. यानी अब तकनीक सिर्फ समय से पहले जन्मे बच्चों को बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह जीवन की शुरुआत को ही नियंत्रित कर सकती है. वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले 10 वर्षों में इसका सीमित प्रयोग इंसानी नवजात शिशुओं के लिए भी संभव हो सकता है, हालांकि पूरी तरह से कृत्रिम मानव गर्भ के लिए अभी और रिसर्च और नैतिक विमर्श की जरूरत है.
जापान में ही क्यों हुई यह क्रांति?
जापान में इस तकनीक का सामने आना कोई इत्तेफाक नहीं है. यह देश पिछले कई सालों से जनसंख्या संकट से जूझ रहा है. 2024 में जापान में अब तक की सबसे कम जन्म दर दर्ज हुई. युवाओं की संख्या घट रही है, बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है और नई पीढ़ी बच्चों की जिम्मेदारी लेने में हिचक रही है. सरकार ने नकद सहायता, माता-पिता की छुट्टी और चाइल्ड केयर जैसी कई योजनाएं शुरू कीं, लेकिन बदलाव नहीं आया. ऐसे में जब पारंपरिक रास्ते विफल हो गए, तो जापान ने विज्ञान की ओर रुख किया. कृत्रिम गर्भ उसी दिशा में एक बड़ा और साहसी कदम है जो विज्ञान को जनसांख्यिकीय संकट का समाधान बना रहा है.
महिलाओं के लिए वरदान या चुनौती?
इस तकनीक को देखकर कुछ लोग कह सकते हैं कि यह कामकाजी महिलाओं के लिए वरदान है. अब उन्हें मां बनने के लिए करियर छोड़ने या शारीरिक जोखिम उठाने की ज़रूरत नहीं होगी. लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या यह तकनीक गर्भधारण की सुंदरता और भावनात्मक जुड़ाव को खत्म कर देगी? क्या ‘मां’ शब्द सिर्फ एक बायोलॉजिकल टर्म बनकर रह जाएगा? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह तकनीक महिलाओं को विकल्प देती है, जबकि कुछ को लगता है कि यह मातृत्व की भावनात्मक गहराई से वंचित कर सकती है. यह एक सामाजिक और भावनात्मक बहस है जो अब शुरू हो चुकी है.
क्या मशीनें ले लेंगी इंसानों की जगह?
गर्भावस्था हमेशा एक ऐसा समय रहा है जिसमें मां और बच्चे के बीच गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनता है. यह जुड़ाव सिर्फ जैविक नहीं होता, बल्कि सामाजिक, मानसिक और आत्मिक होता है. अगर यह सब लैब और मशीनों से किया जाने लगे, तो क्या हम उस मानवीय अनुभव को खो देंगे? क्या आने वाली पीढ़ी सिर्फ जैविक रूप से नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी अलग होगी? कई आलोचक मानते हैं कि तकनीक हमें सुविधा दे सकती है, लेकिन भावनात्मक गहराई शायद खो दे.
पेरेंटिंग पर उठेंगे कई सवाल
कृत्रिम गर्भ के ज़रिए पेरेंटिंग अब सिर्फ स्त्रियों का विषय नहीं रह जाएगा. पुरुष, ट्रांसजेंडर, सिंगल लोग और समान-लिंग वाले जोड़े भी जैविक माता-पिता बन सकेंगे. सरोगेसी की ज़रूरत खत्म हो सकती है और परिवार बनाने की परिभाषा पूरी तरह से बदल सकती है. पर क्या समाज इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार है? क्या हमारी कानूनी व्यवस्था यह तय कर पाएगी कि बिना मां के गर्भ के पैदा हुए बच्चे की कानूनी स्थिति क्या होगी? ये सभी सवाल अब हमारे दरवाज़े पर दस्तक दे रहे हैं.
विवादों और डर की भी शुरुआत
इस तकनीक ने जितनी उम्मीदें जगाई हैं, उतने ही डर भी पैदा किए हैं. अगर इस सिस्टम में तकनीकी खराबी आ जाए, या हैकिंग हो जाए, तो क्या भ्रूण को नुकसान होगा? और ऐसी स्थिति में ज़िम्मेदार कौन होगा- वैज्ञानिक, लैब या माता-पिता? साथ ही यह भी खतरा है कि कहीं ये तकनीक सिर्फ अमीरों की पहुंच तक सीमित न हो जाए, और गरीब परिवार इससे वंचित रह जाएं. इससे समाज में एक नया “जन्म आधारित भेदभाव” भी जन्म ले सकता है.
बच्चे को मिलेगी सामाजिक मान्यता?
आज भी दुनिया के ज़्यादातर देशों में ऐसा कोई स्पष्ट कानून नहीं है जो कृत्रिम गर्भ से पैदा होने वाले बच्चों की स्थिति को स्पष्ट करता हो. क्या उन्हें मां की कोख के बिना भी समान अधिकार मिलेंगे? क्या उनके जन्म को सामाजिक मान्यता मिलेगी? और अगर भविष्य में कोई भ्रूण केवल शोध के लिए विकसित किया जाए, तो क्या वह नैतिक होगा? ऐसी तमाम जटिलताएं हैं जिनके लिए हमें एक सामूहिक और पारदर्शी संवाद की ज़रूरत है.
विज्ञान की क्रांति या इंसानियत की परीक्षा?
जापान की यह तकनीक न सिर्फ विज्ञान में क्रांति है, बल्कि इंसानियत, नैतिकता और समाज के सामने एक बहुत बड़ा आईना भी है. यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम जीवन को कैसे देखते हैं. क्या वह सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया है या भावनात्मक यात्रा? क्या हम इसे मशीनों के हवाले कर सकते हैं या फिर हमें कुछ सीमाएं तय करनी होंगी? यह शुरुआत तो हो चुकी है, अब यह हम पर है कि हम इसे किस दिशा में लेकर जाते हैं- सुविधा की ओर, संवेदना की ओर या संतुलन की ओर.